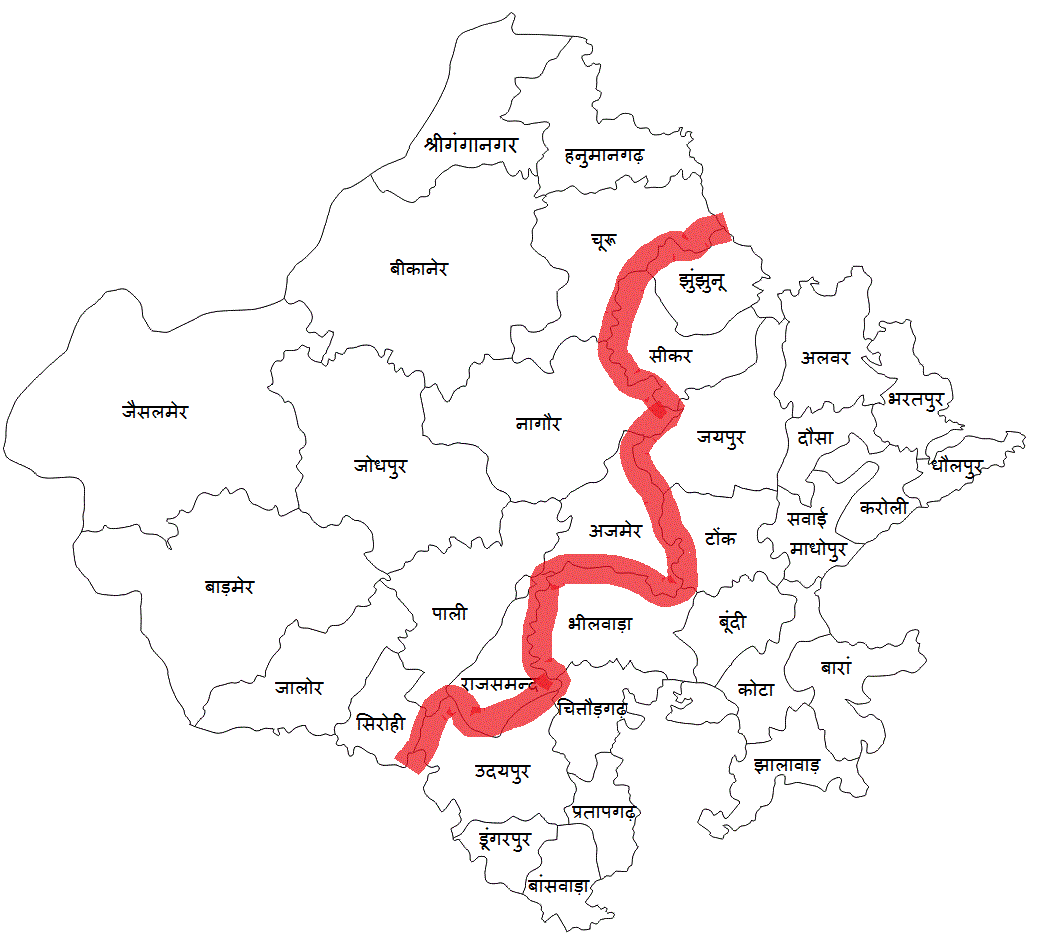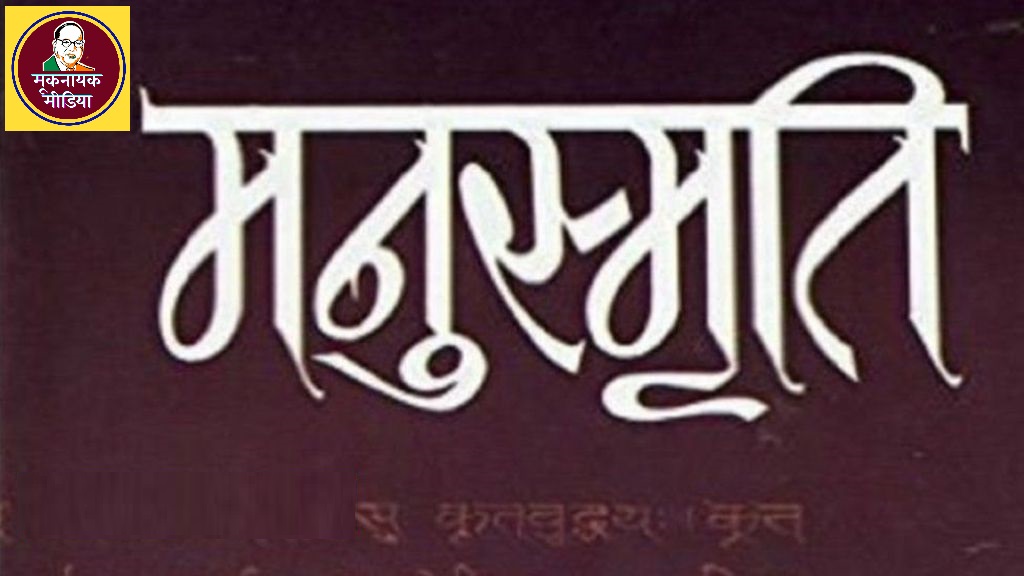
मूकनायक मीडिया ब्यूरो | 05 जुलाई 2024 | जयपुर : यदि आदि संविधानकार मनु है तो वैदिक साहित्य से चार गुना बड़ा बौद्ध पाली साहित्य में मनु का कोई नामों-निशान क्यों नही है…?? बाबासाहब जी का मनु से कोई ख़ास विरोध था न ही अन्य किसी ब्राम्हण साहित्य से, मनु का विरोध खुद हिंदुओं और ब्राह्मणों का था। जो आर्य समाज या सत्य शोधक समाज से संबंधित थे चुकी बाबासाहब जी के पिता रामजी अंबेडकर के तत्वनिष्ठ सत्य शोधक समाज से मैत्री सम्बंध थे।
इस कारण आर्य समाज का एक गुट बाबासाहब जी से संवेदनशील था इसीलिए उन्होंने 1936 में लाहोर के ज़ात पात तोड़क मण्डल के सम्मेलन में बाबासाहब को अध्यक्षता का अनुरोध किया था। इसी तरह सत्यशोधक समाज के कई ब्राम्हण कार्यकर्ताओ के और बाबासाहब के निकट मित्रता पूर्ण संबंध थे।

इसीके चलते 1927 में महाड़ (नाशिक) के( ब्रम्ह ण) बापूसाहेब सहस्त्र बुद्धे की अध्यक्षता में मनुस्मृति दहन का आयोजन किया गया। ज्ञात हो मनु के सबसे बड़े दुश्मन बाबासाहब नही बल्कि फुले है फुले ने ही मनुस्मृति जलाने योग्य है इस तरह का ज़िक्र अपनी ‘अखण्डदि’ नामक पुस्तक में किया है। प्रचलित वर्ण-व्यवस्था का मूलाधार मनुस्मृति है।
क्या मनुस्मृति में वर्णित वर्णव्यवस्था व्यावहारिक है?
मनुस्मृति की रचना बहुत अर्वाचीन है, यह सभी ऐतिहासिकों का मत है। मनुस्मृति मनु की बनाई हुई है-ऐसा मानना भी एक बड़ी भारी भूल है। मनु के नाम से किसी दूसरे ने ही इस भयंकर पुस्तक की रचना कर दी है। तभी आज कल सभी मनुस्मृतियों में यह श्लोक पाया जाता है- इत्येतत् मानवं शास्त्रं भृगुप्रोक्तं सनातनम् अर्थात् यह भृगुऋषि की कही हुई है। शूद्रों को पूर्ण रूप से पददलित कराने वाले मनुस्मृति के 10वें अध्याय का निचोड़ सत्यार्थ प्रकाश के 10 समुल्लास में विद्यमान है।
स्वामी दयानन्द जैसे आदर्श सुधारक लिखते हैं कि- शूद्र लोग आर्यों के घर में जब रसोई बनावें तब मुख बाँध के बनावें क्योंकि उनके मुख से उच्छिष्ट और निकला हुवा श्वास भी अन्न में न पड़े। मनुस्मृति के 10वें अध्याय में कितना भारी षड्यन्त्र है उसका नमूना इस एक श्लोक में और पढ़ लीजिए। ‘यो लोभात् अधमो जात्या जीवेत् उत्कृष्ट कर्मभिः।’ तें राजा निर्धनं कृत्वा क्षिप्रमेव विवासयेत्॥10/96॥ अर्थात् जो शूद्र, अछूत या शिल्पी जीविका के लोभ से अच्छे कर्मों द्वारा अपने जीवन को बिताने लगे तो राजा इन सबका धन छीन ले और तुरन्त देश से निकाल देवें। कैसा रौलेट एक्ट बनाया है।
वर्णाश्रम का इतिहास चारों वेदों में कहीं भी वर्ण पद का उल्लेख नहीं मिलता है। सर्वप्रथम वर्ण पद भगवद्गीता में पाया गया है, जो निम्न प्रकार हैः- ‘चातुवर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः’ (४/१३) श्लोक के इस अंश में परमेश्वर द्वारा गुण और कर्म के आधार पर चार वर्णों की सृष्टि किया जाना बताया गया है। यदि हम महाभारतकाल में उपलब्ध वर्णव्यवस्था का अध्ययन करें तो पाते हैं कि उस समय भी जाति के आधार पर ही वर्णव्यवस्था थी।गुण और कर्म के आधार पर वर्णव्यवस्था उस समय भी स्थापित नहीं की जा सकती थी।
इस विषय में श्रीवसन्तकुमार चट्टोपाध्याय एम. ए. का कहना है- ‘‘ यदि किसी व्यक्ति की जाति उसकी वृत्ति वा कर्म पर निर्भर होती तो द्रोणचार्य क्षत्रिय कहलाते क्योंकि उनका व्यवसाय युद्ध करना था। पर वे जन्म के कारण ही ब्राहमण थे। उधर द्रोण-पुत्र अश्वत्थामा में कोई भी गुण-कर्म ब्राहमण जैसे न थे। क्रूर स्वभाव था। कर्म क्षत्रिय का करते थे।
पांडवों के शिविर मे द्रौपदी के पुत्रों का वध करने पर जब वे पकड़े गए तो उन्हें ब्राहमण मान कर मृत्युदण्ड नहीं दिया गया, केवल उनका सिर मूडकर निष्कासित कर दिए गए थे। युधिष्ठर ब्राहमण स्वभाव के थे। जघन्य अपराधी को भी क्षमा कर देते थे। भीम तो जरा सी बात पर युद्ध को तैयार हो जाते थे। यदि गुणों को वर्णों का कारण माना जाता तो दोनों का पृथक्-पृथक् वर्ण मानना चाहिए था।
पर थे दोनों क्षत्रिय ही। कर्म से वर्ण परिवर्तन कब हुआ ?’’ उक्त तथ्यों से यह प्रमाणित होता है कि महाभारत काल में जन्मना जाति व्यवस्था लागू थी। गीता के अनुसार वर्णाश्रम धर्म का पालन करने में लाभ और परिवर्तन से हानि- गीता में कहा गया है- स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः (१८/५४) अर्थात् अपने ही वर्णधर्म के पालन में मनुष्य की उन्नति होती है।
गीता में ही कहा गया है- श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात्स्वनुष्ठितात्। स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः।। (३/३५) अर्थात् सुन्दर रूप से अनुष्ठित परधर्म की अपेक्षा गुण रहित होने पर भी निजधर्म श्रेष्ठतर है अपने (वर्णाश्रम) धर्म में मृत्यु भी कल्याणकारी है, दूसरों का धर्म भययुक्त या हानिकारक है।
गीता में ही अन्यत्र कहा गया है –संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च। (१/४२) अर्थात् वर्ण-संकरता कुल नष्ट करने वालों को और कुल दोनों को निश्चय से नरक में ले जाती है। इस श्लोक के अगले श्लोक में कहा गया है- दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः। उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः।। (१/४३)
अर्थात् कुल का हनन करनेवाले लोगों के वर्ण-संकरता उत्पन्न करने वाले इन दोषों के कारण जाति-धर्म तथा सदा से चले आ रहे कुल-धर्म नष्ट हो जाते हैं- न समाज की परम्पराएं बनी रहती हैं, नकुल की परम्पराएं बनी रहती हैं। महाभारत काल में यदि वर्ण और जातिभेद जन्म से नहीं था तो गीता में कुल धर्म और जाति धर्म की बात कहां से आ गई ? वर्ण व्यवस्था का विधान स्मृतियों, विशेष रूप से मनुस्मृति में है।
जन्मजात वर्णव्यवस्था से हानियां–
- जन्म से वर्ण मानने से एक वर्णवाले मनुष्य के लिए दूसरे वर्ण में प्रवेश के द्वार सदा के लिए बन्द कर दिए जाते हैं।
- मनुष्यों में जात्याभिमान उत्पन्न होता है और वे बिना गुण व योग्यता के भी अपने को अन्यों से श्रेष्ठ समझने लगते हैं।
- जात्याभिमान के कारण समाज में द्वेष और घृणा उत्पन्न होती है।
- शूद्र अपने अच्छे गुण, कर्म, सदाचार और भक्ति से भगवान् को प्राप्त कर सकता है, परन्तु कभी शूद्र से ब्राहमण नहीं बन सकता है।
जाति व्यवस्था का संक्षिप्त इतिहास जैसा कि उपरोक्त रूप से उल्लिखित किया गया है कि महाभारत काल में भी वर्णव्यवस्था न होकर जाति व्यवस्था लागू थी। महाभारत के बाद तो गुण-कर्म का आधारपूर्ण रूप से विलुप्त हो गया। मनु ने ऐसे ब्राहमणों का वर्णन किया है जो पतित, नास्तिक और नपुंसक थे। (मनुं २/१५०) अब गुण-कर्म की कसौटी को तिरोहित कर दिए जाने के बाद वर्ण का निर्धारण जन्म के आधार पर ही किया जाने लगा। उसके बाद तो ऊँच-नीच का भेद और भी बढ़ने लगा।
सूत्र ग्रन्थों की रचना के समय तो उन्हें अत्यन्तहीन और नीच समझा जाने लगा था। गौतम धर्मसूत्र (१२-४) के अनुसार यदि ‘‘शूद्र वेद मंत्र का उच्चारण करे तो उसकी जीभ काट देनी चाहिए। यदि वेद को याद करे तो उसका शरीर चीर डालना चाहिए।’’ बुद्ध के प्रादुर्भाव के समय तक भारत के सामाजिक संगठन का रूप अत्यन्त विकृत हो गया था।
बौद्ध साहित्य में इसी कारण से वर्णभेद की कटु आलोचना की गई है। जैन धर्म के प्रवर्त्तक वर्धमान महावीर भी इस व्यवस्था के कटु आलोचक थे। बौद्ध और जैन धर्म के प्रवर्त्तकों ने इन बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया परन्तु उन्हें सीमित सफलता ही प्राप्त हो सकी थी।
बुद्ध ने अपने समय में वर्तमान जन्मना जाति व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाई और जन्म के आधार पर किसी को उच्च या नीच नहीं माना परन्तु जन्मना जाति व्यवस्था पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और जातिव्यवस्था पहले की तुलना में अधिक विकृत हो गई। महर्षि पतंजलि (२०० ईं० पूं०) के समय तक जाति व्यवस्था का स्वरूप और अधिक विकृत हो चुका था।
पतंजलि ने शूद्रों के महाभाष्य (२/४/१०) में दो भेद किए हैं- ‘‘ एक अबहिकृत और दूसरे बहिकृत। तक्षा और अयस्कार आदि जो द्विजों के बर्तन छू सकते थे, अबहिकृत या अनिरवसित जो द्विजों के पात्र नहीं छू सकते थे, चाण्डाल और मृतप आदि निरवसित या बहिकृत शूद्र थे।’’ समय के साथ-साथ वर्णभेद अत्यन्त संकीर्ण और कठोर हो गया।
जातीय भेदभाव को मिटाने के प्रयास– समय-समय पर अनेक महापुरुषों ने जातीय भेदभाव को मिटाने और समाज में समानता लाने के प्रयत्न किए। इन महापुरुषों का कहना था कि अच्छे गुण, कर्म, सदाचार और भक्ति से मनुष्य ऊँचा पद प्राप्त कर सकता है।
गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर अपने प्रयासों में आंशिक रूप से ही सफल हो पाए थे। अन्य महापुरुषों में रामानन्द, चैतन्य, नानक, कबीर आदि प्रमुख थे। ये सन्त महात्मा भी हिन्दू समाज में व्याप्त ऊँच-नीच और छूत-अछूत की घोर समस्या का निदान नहीं कर सके थे। उन्नीसवीं शती के पूर्वाद्ध में इस देश में नवजागरण का सूत्रपात हुआ। इस समय पर समाज सुधार के क्षेत्र में ब्राहमसमाज, थियोसोफिकल-सोसाइटी और प्रार्थना
समाज ने मुख्य रूप से ऊँच-नीच और छूत-अछूत की घोर समस्या का निदान करने का प्रयास किया। प्रार्थनासमाज जिसकी स्थापना १८६७ में हुई थी के लोग जाति-प्रथा उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देते थे और बाल-विवाह निषेध का प्रचार करते थे। ये लोग कुरीतियों के विरोध में घोर आन्दोलन करते थे तथा सुधार चाहते थे परन्तु व्यवहार में, इनके हिन्दू समाज के कर्मकाण्डों में उलझे होने के कारण सामाजिक सुधार के क्षेत्र में इनका प्रभाव नगण्य रहा।
इसी प्रकार ब्राहमसमाज और थियोसोफिकल-सोसाइटी भी जाति-प्रथा उन्मूलन के सम्बन्ध में कोई विशेष प्रगति नहीं कर पाए थे। ऐसे समय पर ऊँच-नीच और छूत-अछूत की घोर समस्या का निदान करने और वर्णाधारित समाज की स्थापना हेतु उन्नीसवीं शती में महर्षि दयानन्द सरस्वती और उनके द्वारा स्थापित संगठन आर्य समाज ने इस क्षेत्र में पदार्पण किया।
महर्षि दयानन्द सरस्वती और आर्यसमाज द्वारा किए गए प्रयास– महर्षि दयानन्द सरस्वती और आर्यसमाज गुण, कर्म और स्वभाव से वर्णव्यवस्था स्वीकार करता है, जन्म से नहीं। इसका आधार यजुर्वेद का यह प्रसिद्ध मंत्र है- ब्राहमणोऽस्य मुखमासीद् बाहू राजन्य कृतः। ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रोऽजायत।। (३१/११)
पौराणिकों द्वारा उक्त मंत्र का अर्थ निम्न प्रकार किया गया है- ब्राहमण परमात्मा के मुख से उत्पन्न हुए, क्षत्रिय उसकी बाहों से, वैश्य जंघाओं से और शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए। महर्षि दयानन्द ने अपने कालजयीग्रन्थ सत्यार्थप्रकाश में उक्त मंत्र के सम्बन्ध में निम्नप्रकार व्याख्या की है- व्याख्या– इस मंत्र का जो तुमने अर्थ किया है वह ठीक नहीं, क्योंकि यहां पुरुष अर्थात् निराकार, व्यापक परमात्मा की अनुकृत्ति है।
जब वह निराकार है तो उसके मुखादि अंग नहीं हो सकते, जो मुखादि अंग वाला हो तो वह पुरुष अर्थात् व्यापक नहीं।और जो व्यापक नहीं वह सर्वशक्तिमान् जगत् का स्रष्टा, धर्त्ता, प्रलयकर्त्ता, जीवों के पुण्य-पापों को जान के व्यवस्था करने हारा, सर्वज्ञ, अजन्मा, मृत्यु रहित आदि विशेषण वाला नहीं हो सकता, इसलिए इसका अर्थ है कि जो (अस्य) पूर्णव्यापक परमात्मा की सृष्टि में मुख के सदृश सब में मुख्य उत्तम हो वह ब्राहमण (बाहू) बाहुर्वैबलम्; (५/४/१/१) बाहुर्वैवीर्यम्; (६/३/२/३५) शतपथब्राहमण।
बल-वीर्य का नाम बाहु है, वह जिसमें अधिक हो सो (राजन्यः) क्षत्रिय (ऊरू) कटि के अधोभाग और जानु के उपरिस्थ भाग का नाम ऊरू है, जो सब पदार्थों ओर सब देशों में जावे-आवे, प्रवेश करे वह (वैश्यः) वैश्य और (पद्भ्याम्) जो पग के अर्थात् नीच अंग के सदृश मूर्खत्वादि गुणवाला हो वह शूद्र है।
अन्यत्र शतपथ-ब्राहमणादि में भी इस मंत्र का ऐसा ही अर्थ किया है। महर्षि ने न केवल गुण, कर्म और स्वभाव से वर्णव्यवस्था स्वीकार की अपितु मनुस्मृति के निम्न श्लोक को उवरित करते हुए यह भी कहा कि जो शूद्र कुल में उत्पन्न होके ब्राहमण, क्षत्रिय और वैश्य के समान गुण, कर्म और स्वभाव वाला हो तो वह शूद्र, ब्राहमण, क्षत्रिय और वैश्य हो जाय, वैसे ही जो ब्राहमण, क्षत्रिय और वैश्य कुल में उत्पन्न हुआ हो और उसके समान गुण, कर्म और स्वभाव शूद्र के सदृश हों तो वह शूद्र हो जाय, वैसे क्षत्रिय वा वैश्य के कुल में उत्पन्न होके ब्राहमण, ब्राहमणी वा शूद्र के समान होने से ब्राहमण और शूद्र भी हो जाता है, अर्थात चारों वर्णों में जिस-जिस वर्ण के सदृश जो-जो पुरुष वा स्त्री हो वह-वह उसी वर्ण में गिनी जावे।
शूद्रो ब्राहमणतामेति ब्राहमणश्चैति शूद्रताम्। क्षत्रियाज्जातमेवन्तु विद्याद्वैश्यात्तथैव च।। मनुं (१०/६५) महर्षि दयानन्द सरस्वती ने यह प्रतिपादित किया कि सब बालक और बालिकाओं को शिक्षा का समान अवसर दिया जाना चाहिए। चाहे वे किसी भी वर्ण या कुल में उत्पन्न हुए हों। स्त्रियों और शूद्रों को शिक्षित करने का उन्होंने प्रबल समर्थन किया।
उन्होंने कहा कि सब मनुष्यों को वेदादि शास्त्र पढ़ने का अधिकार है और अपने कथन के समर्थन में यजुर्वेद का निम्न मन्त्र प्रस्तुत कियाः- यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः। ब्रहमराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय।। (२६/२) महर्षि का यह मानना था कि जन्म से सब शूद्र होते हैं, शिक्षा और संस्कार से ही द्विज बनते हैं।
आर्यसमाज का इतिहास, प्रथम भाग-पृष्ठ-४४५ (प्रधान सम्पादक- डां सत्यकेतु विद्यालंकार) पर महर्षि के विचार निम्न प्रकार वर्णित हैं- ‘‘ महर्षि ने प्रतिपादित यह किया, कि विद्या सबके लिए है और सबको ज्ञान प्राप्ति का एक समान अवसर दिया जाना चाहिए, और शिक्षा की समाप्ति पर ही यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि अपनी योग्यता और गुणों के कारण कौन व्यक्ति किस वर्ण में होने के योग्य है। जब वर्ण निर्धारित हो जाए, तो सबको उनके वर्णों के अनुरूप कार्य भी दिया जाना चहिए। ’’
महर्षि अपने जीवन में सदैव जन्मना जातीय व्यवस्था के उन्मूलन और छुआछूत दूर करने के लिए संघर्षरत रहे और उनके द्वारा स्थापित संगठन आर्य समाज ने भी उन्नीसवीं शती के अन्तिम वर्षों और बीसवीं शती के कुछ वर्षों तक सामाजिक कुरीतियों और विषमताओं के विरुद्ध सशक्त आन्दोलन किया जिसके फलस्वरूप जातीय विषमता में काफी गिरावट भी हुई परन्तु धीरे- धीरे आर्यसमाज का यह आन्दोलन शिथिल पड़ने लगा और आज तो यह स्थिति आ चुकी है कि यह महारोग आर्यसमाज के किसी एजेन्डा में भी नहीं है।
इसका कारण आर्यसमाज के केन्द्रीय और प्रान्तीय संगठनों का आपसी फूट या अन्य कारणों से कमजोर हो जाना या समाज के प्रति संवेदनहीन हो जाना भी हो सकता है।जहां कहीं इस दिशा में कोई कार्य हो रहा है, वह कतिपय आर्यजनों या श्रेष्ठ आर्यसमाजों के निजी प्रयासों से ही कार्य किया जा रहा है।
वेद प्रचारिणी सभा नागपुर का नाम एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में रखा जा सकता है जो समय-समय पर सम्मेलन/गोष्ठियों और प्रचार कार्य करके महर्षि के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। आज तो स्थिति यह लगती है कि आर्यसमाज के अधिकांश सदस्य भी जातीयता के घेरो से बाहर नहीं निकले प्रतीत होते हैं क्योंकि महर्षि द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों पर चलता हुआ शायद ही कोई दिखाई दे।
आर्यसमाज ने दलित व पिछड़े समाज से जो व्यक्ति विद्वान् या पुरोहित के रूप में बनाए थे, उन्हें स्वयं के विवाह के लिए और उनकी सन्तानों के विवाह के लिए भी समस्याओं का सामना करना पडा़ क्योंकि आर्य या तथाकथित आर्य तो अपने जन्मना जातीय कुलों में ही विवाहादि करते हैं।
पौराणिक लोगों से तो कभी भी यह अपेक्षा नहीं थी कि वे निम्नवर्ण से उच्च वर्ण में किसी को प्रोन्नत होता हुआ देख सकेंगे। आर्यों ने भी कभी वर्णों के उच्चीकरण में कोई सहायक भूमिका नहीं निभाई। यदि वर्णों का निर्धारण समावर्त्तन संस्कार के समय ही किया जाना होता है और महर्षि ने स्वयं ऐसा विधान भी किया है, जैसे कि उपराक्त रूप से वर्णित किया गया है तो आर्य समाज के संगठन के गुरुकुलों में तो कम से कम महर्षि के निर्देशों के अनुरूप शिक्षापूर्ण करनेवाले विद्यार्थियों को क्रमशः ब्राहमण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण का घोषित किया जाना चाहिए।
मनुस्मृति का विधान हजारों वर्ष से चला आ रहा है जिसे महिमा मण्डित करने में और जिसका औचित्य सिद्ध करने में हमारे आर्यसमाज के विद्वानों ने भी हजारों पृष्ठ का लेकर दिए परन्तु व्यवहार के धरातल पर वे एक भी ऐसा उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं जिसे आधुनिक समय में किसी को गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर शास्त्रों में वर्णित विधि के अनुसार ब्राहमण, क्षत्रिय या वैश्य घोषित किया गया हो।
ऐसे में गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर हमारे द्वारा मानी जा रही यह व्यवस्था हाथी के दिखावटी दांतों के सदृश ही मानी जायेगी क्योंकि खाने के दांत भिन्नहैं। महर्षि स्वयं वर्णव्यवस्था के वर्तमान स्वरूप से दुःखी थे। उन्होंने जन्म मूलक वर्ण व्यवस्था पर कुल्हाड़ा चलाया।
बाद में जब उन्होंने अनुभव किया कि जन्म हो कर्म से, यह वर्णव्यवस्था समाज के लिए घोर हानिकारक है तो उन्होंने साफ कह दिया -‘‘यह वर्णव्यवस्था तो आर्यों के लिए मरणव्यवस्था बन गई है। देखें इस डाकिन से कब पीछा छूटता है।’’ (अन्तर्राष्टीय आर्य समाज स्मारिका, पृष्ठं ६४) महर्षि के उक्त कथन के परिप्रेक्ष्य में यह विचार करना आवश्यक है कि क्या मनुस्मृति पर आधारित वर्णव्यवस्था आज के समय में व्यावहारिक है? मनुस्मृति पर आधारित वर्णव्यवस्था की व्यावहारिक प्रासंगिकता– १. गुण कर्मों से किसी का वर्ण निश्चित करना अति दुष्कर कार्य है क्योंकि किसी मनुष्य के गुण तो उसे एक वर्ण का बताते हैं परन्तु कर्म दूसरे अन्य वर्ण के होते हैं।
आधुनिक समय में यह भी होता है कि एक व्यक्ति कृषि कार्य करता है और विद्यालय में या निजी स्तर पर घर पर ही बालक-बालिकाओं को शिक्षित करने का व्यवसाय भी करता है। एक व्यक्ति सैनिक है और सेना में पुरोहित का भी कार्य करता है। भारत के कई सेना के जनरल, नौ-सेना के एडमिरल और वायु सेना के अध्यक्ष ऐसे हुए हैं जिन्होंने ब्राहमणों के घर जन्म लिया, जीवन भर सेना में कार्यरत रहने के बाद भी वे क्षत्रिय नहीं हुए और ब्राहमण ही कहलाये।
यही स्थिति अन्य सैनिकों की भी रहती है। जीवनभर कृषि कार्य करने वाले ब्राहमण-जन्मना कभी वैश्य नहीं हो पाए। ऐसी दशा में वर्ण कैसे निश्चित होगा? फिर इस बात का भी कोई भरोसा नहीं है कि वर्तमान गुण, कर्म या व्यवसाय आजीवन वैसे ही बने रहेंगे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा।
यदि ये बदल गए तो वर्ण भी परिवर्तित करना पड़ेगा। साथ ही दो या दो से अधिक भिन्न-भिन्न व्यवसाय करने वालों का वर्ण कैसे निर्धारित किया जायेगा? २. संसार में २२० से अधिक देश हैं जिनमें से भारत, नेपाल, बंगलादेश, पाकिस्तान आदि में जहां हिन्दू निवास करते हैं जाति व्यवस्था है, अन्य देशों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, फिर भी वहां बुद्धिजीवियों का कार्य, देश की रक्षा का कार्य, वाणिज्य व कृषि और सेवाकार्य सुचारू ढंग से चलता है।
वहाँ पर कोई जातीय वैमनस्य या उसका कोई कारण भी नहीं है। केवल भारत में ही मनुष्यों को विभाजित करने वाले इस विधान का क्या औचित्य है ? ३. भारत में प्रजातंत्र है और इस प्रजातंत्रीय व्यवस्था में मनुष्यों के जीवन को जीने के लिए अधिकार और कर्तव्य संविधान में दिए गए हैं।
संविधान मनुष्यों को समान अधिकार देता है। ऐसे में भी गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर उन्हें विभाजित करना विधि अनुकूल नहीं है। हिन्दुओं में दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों की जनसंख्यां प्रतिशत से अधिक है, ऐसे में आर्यसमाज द्वारा मनुस्मृति की इस व्यवस्था को मानने के कारण अधिकांश हिन्दू आर्य समाज के अन्य गुणों को जानते और मानते हुए भी इसकी ओर आकर्षित नहीं होते, इसके विपरीत इसकी निन्दा करने पर उतारू हो जाते हैं।
महर्षि को यदि और अधिक जीवनकाल मिला होता और वे अपने उक्त निष्कर्ष पर पुनः मनन करते तो क्या फिर भी मनुस्मृति आधारित वर्णव्यवस्था लागू करने का परामर्श देते, यह विचारणीय है। समस्त आर्यजनों से निवेदन है कि कृपया महर्षि के जीवन के उक्त निष्कर्ष और लेख में प्रस्तुत बिंदुओं के आधार पर विचार करें कि क्या मनुस्मृति में वर्णित वर्ण व्यवस्था व्यावहारिक है?
बिरसा अंबेडकर फुले फातिमा मिशन को आगे बढ़ाने के लिए ‘मूकनायक मीडिया’ को आर्थिक सहयोग जरूर कीजिए